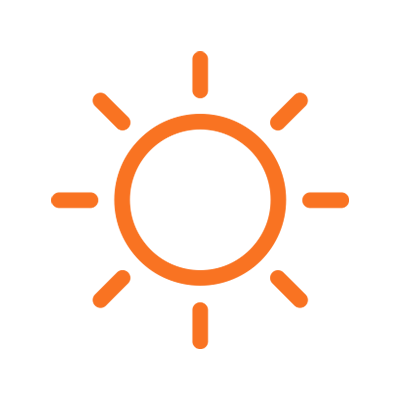गुरबचन जगत
राज्यसभा चुनावों से पहले, कुछ सूबों में राजनीतिक माहौल देखकर वास्तव में दुख और निराशा हुई। ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ नया हुआ लेकिन यह तथ्य है कि नैतिकता किस कदर पराभव के गर्त में गिरती जा रही है और इस गिरावट के थमने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। चूंकि इस कुएं का तल नहीं है इसलिए लगता है हम सदा के लिए नीचे ही नीचे धंसते जा रहे हैं। चुनाव का मामला सरल गणित होता है यानी यदि आपके पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं तो सदन की सीट जीत लेंगे, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई हाथ में वोटों से ज्यादा सीटें पाना चाहे। तब नए समीकरण बैठाए जाते हैं, जिसके मुख्य अवयवों में धन-शक्ति, बाहुबल और संस्थागत भ्रष्टाचार है। इन तमाम ‘गुणों’ का खुलकर प्रदर्शन होता है। फिर देश में ऐसे मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष हैं, जिनकी महारत दूसरे दलों के नेताओं काे निशाना बनाने की है, वे तोड़कर लाए नेता को अपने बेहतरीन ‘आखेट के नमूने’ की तरह प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं कि जिन पार्टियों के पास जीतने लायक संख्या नहीं होती वे अमीर चेहरों को खड़ा करती हैं। यह उन्हें विधायकों की मंडी में दाखिल होकर अपने लिए पर्याप्त वोट खरीदने का आमंत्रण होता है। फिर यह धनकुबेर गर्व से दावा करते हैं कि उन्होंने जीत पर्याप्त संख्या में वोट लेकर पाई है। फिर ऐसे भी हैं जो निर्विरोध चुने जाते हैं, जिनको पर्याप्त विधायक संख्या बल वाले दल प्रायोजित करते हैं, उनमें कुछ उन सूबों से नहीं होते, जहां चुनाव हो रहे हों। इसमें गड़बड़ क्या है- इस बाबत आपका अंदाजा भी मेरे जितना सही है।
वे ‘भद्र लोग’ जो पाला बदल लेते हैं, क्या उनका किसी विचारधारा के प्रति झुकाव है? यदि है, तो क्या उन्होंने नई पार्टी की विचारधारा को अधिक लुभायमान पाकर पाला बदला? यह और कुछ नहीं, केवल ताकत और धन-दौलत का गलीज खिंचाव है। यही बात उन दलों के लिए भी सही है जो उन्हें डोरे डालते हैं और उनकी वोट स्वीकार करते हैं। जहां कहीं ये तमाम पैंतरे असफल रहते हैं, तब तकनीकी बिंदु उठाए जाते हैं, संस्थागत मदद ली जाती है क्योंकि शुरू से ही सत्ता ऐसे संस्थानों में प्रभावशाली पद पर बैठने वालों को फायदा पहुंचाती आई है। तो हमारे पल्ले है क्या? क्या हमारे पास संसद का वह उच्च सदन है, जिसमें विलक्ष्ण बुद्धिमत्ता और नैतिकता से परिपूर्ण शख्सियतें हों, जो लोकसभा द्वारा उनको भेजे गए मामलों पर माकूल बहस और विमर्श करने की काबिलियत रखते हों और फिर अपने अनुभव से सलाह दे सकें – जी नहीं जनाब। वहां तो अधिकांश वे लोग बैठे हैं जो संकेत मिलने पर हाथ उठाकर या तो ‘आए-आए’ करते हैं या फिर ‘हाय-हाय’ करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब अभी हो रहा है –आरंभ में, अपनी लीक बनाने वालों में एक इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने ‘सिंडीकेट’ कहे जाने वाले पुराने कांग्रेसियों को निकाल बाहर करने की खातिर कांग्रेस को दोफाड़ किया। इंदिरा ने राष्ट्रपति पद के लिए वीवी गिरी को बतौर आजाद उम्मीदवार खड़ा किया और उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी को हरा दिया। फिर चौधरी चरण सिंह की छिपी महत्वाकांक्षा जगी और उन्होंने मोरारजी देसाई और जनता पार्टी की सरकार गिरा दी, और कांग्रेस (आई) के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। आगे चलकर कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, तदनुसार इंदिरा गांधी 1980 में फिर प्रधानमंत्री बनीं।
नई लीक बनाने वाले उपरोक्त नेताओं के बाद आए उनसे भी बड़े मौकापरस्त। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं तब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल अपने अधिकांश मंत्रियों और विधायकों समेत जनता पार्टी से टूटकर कांग्रेस (आई) में शामिल हुए। सत्ता के खेल में भजन लाल का नाम सबसे बड़े रणनीतिकारों में आता है। उनका एक कथन है : ‘राजनीति में कोई या तो संन्यास ले ले या फिर सही घड़ी पर सही निर्णय ले’। आगे चलकर वह समय भी आया, ‘जब राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है’ के नारे से पुकारे जाने वाले वीपी सिंह आए, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता दल के कंधों पर सवार होकर प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार तब गिरी जब भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और जनता दल से टूटे धड़े का नेतृत्व करने वाले चंद्रशेखर भारत के नए प्रधानमंत्री बन गए, जिन्हें कांग्रेस का बाहरी समर्थन मिला। कांग्रेस ने उनसे भी समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई और तब नए आम चुनाव करवाना जरूरी हो गया। राजीव गांधी की हत्या हुई और नरसिम्हा राव अल्प संख्या में सांसद अपने हाथ होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद गोलमाल प्रबंधों वाले काल में देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल छोटी-छोटी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने।
तत्पश्चात, आया वह मशहूर प्रसंग, जब प्रधानमंत्री बनने के चंद दिनों बाद वाजपेयी सरकार दलबदल के कारण गिर गई, यह शख्स थे नेशनल कान्फ्रेंस के एकमात्र सांसद सैफुद्दीन सोज़। इस एक वोट के कारण देश को फिर से आम चुनाव से गुजरना पड़ा। आखिरकार हमें 1999 में स्थिरता वाली सरकार मिली जब वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने, इसके बाद यूपीए गठबंधन ने भी दो स्थिर सरकारें दीं और कार्यकाल पूरा किया। एनडीए और यूपीए की इन स्थिर सरकारों में विभिन्न घटक थे जिनकी जड़ें साझा विचारधारा वाली नहीं थीं। छोटे क्षेत्रीय दलों ने भाजपा और कांग्रेस को बंधक बनाए रखा और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अबाध चलता रहा। आज, हम उस स्थिति में हैं जहां यह नहीं पता कि किस पर यकीन करें।
राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात करें तो इनमें भी कोई देख सकता है कि बड़े परिदृश्य पर वही राज्यसभा वाला अलोकतांत्रिक नाटक खेला जा रहा है। पार्टियों को चुनावी समय का इंतजार रहता है, क्योंकि यही वह वक्त है जब अन्य दलों में तोड़-फोड़ मचाकर उनके नेता अपने पाले में मिलाने का मौसम होता है। आरंभ से देखें तो, दलबदल में कोई विचारधारा शामिल नहीं है क्योंकि अधिकांश दलों के पास इस जैसी वस्तु है ही नहीं। पार्टी नेताओं के लिए घोषणा पत्र जारी करने का अवसर पहले विमोचन, फिर प्रेस वार्ता करते हुए फोटो खिंचवाने का मौका है। मैं किसी ऐसे पार्टी कार्यकर्ता या वोटर को नहीं जानता, जिसने सचमुच इसे पूरा पढ़ा हो। संभावित उम्मीदवारों की छंटाई-सूची सावधानीपूर्वक किए गुणा-भाग के बाद तैयार होती है। कौन लोग पाला बदल सकते हैं उनका मूल्यांकन होता है और उन तत्वों पर पैनी नज़र रखी जाती है जिन्हें टिकट देते वक्त नजरअंदाज किया गया और उनके द्वारा दलबदल की संभावना बहुत हो। जो बड़ी तोपें पाला बदलती हैं वे समर्थकों समेत आते हैं। अक्सर नई पार्टी में उनके आगमन को कुछ इस तरह पेश किया जाता है मानो वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष के फिजूलखर्च बेटे ने घर-वापसी की हो। बौद्धिक एवं नैतिक दिवालियापन की ऐसी नुमाइश और सत्ता एवं पैसे का ऐसा लेन-देन निंदनीय है। यह ऐसे स्तर पर सरेआम हो रहा है जिनसे हम नैतिक व्यवहार की मिसाल पेश करने की उम्मीद रखते हैं।
इस गलीज नाटक का एक अन्य शर्मनाक अंक है, नेतृत्व का यकीन अपने ही विधायकों पर न होना, इसीलिए उन्हें बसों और हवाई जहाजों में भरकर दूर-दराज बने होटलों में बंद कर दिया जाता है ताकि मौकापरस्त तत्व उन्हें बरगला न पाएं। इस वक्त उनकी हालत बाड़े में बंद भेड़ों जैसी दिखाई देती है, जिनको शिकारी भेड़िए उठा न ले जाएं। फिर इन्हें पर्यवेक्षकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी निगरानी तले मतगणना स्थल लाया जाता है, तब भी वे क्रॉसवोटिंग करने का जुगाड़ कर ही लेते हैं।
तो हमारे लिए इससे आगे और क्या है? क्या आपने कभी सुना कि यूके, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे प्रजातंत्रों में विचारधारा और क्रॉसवोटिंग जैसी अलामत पाई गई हो? यहां अगर मैं गलत पाया जाऊं तो खुशी होगी। आमतौर पर दल अपने समर्थकों की वफादारी और विचारधारा के कारण जाने जाते हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है। ऐसे में आपको पता रहता है कि आप किसको वोट डाल रहे हैं और किस लिए। जहां तक मुझे पता है, उपरोक्त वर्णित देशों में कोई दलबदल रोधी कानून नहीं है, उनके यहां हैं तो केवल रिवायतें और दृढ़-निश्चयी नैतिकता। हमारे यहां कानून है लेकिन हमें पता है इसे चकमा कैसे देना है। क्यों नहीं हम ऐसा सरल कानून बना देते, जिसके तहत यदि कोई विधायक दलबदल करे तो इस्तीफा देकर नई पार्टी की ओर से पुनः खड़ा होकर जनादेश प्राप्त करना लाजिमी हो? जब कोई किसी दल में शामिल होता है तो माना जाता है कि ऐसा उसने अपनी बुद्धिमत्ता और अंतरात्मा के स्तर पर किया, तब फिर नई अंतरात्मा कहां से आती है? जब बात मतदाता की आए, तो यह नियम उनपर भी लागू होते हैं। उन्हें भी भली भांति पता होता है कि तमाम चुनावी वादे गर्म हवा वाले गुब्बारों की तरह हैं और मिलना केवल वही है जो चुनाव से पूर्व या उपरांत कुछ मुफ्त की चीज़ों अथवा नकदी के रूप में होगा, इसलिए भाड़ में गई विचारधारा और जो कुछ मिल सके, लपक लो और शुक्रगुजार होकर वोट डालो। कवि हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में कहें तो : ‘यहां सब कुछ बिकता है, दोस्तो रहना ज़रा संभल के… बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं, गुब्बारों में डाल के…।’
लेखक मणिपुर के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर में पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं।