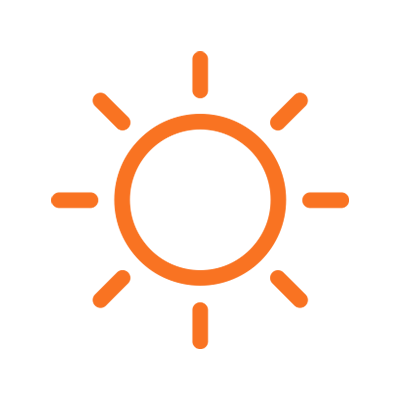पंकज चतुर्वेदी
सीबीएसई बोर्ड की इस घोषणा ने देशभर के किशोरों में घबराहट ला दी कि 15 फरवरी से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहान शुरू होंगे। खुद को बेहतर साबित करने के लिए इन परीक्षाओं में अव्वल नंबर लाने का भ्रम इस तरह बच्चों व उससे ज्यादा उनके पालकों पर लाद दिया गया है कि अब ये परीक्षा नहीं, गला-काट युद्ध सा हो गया है। उधर कई हेल्प लाइन शुरू हो गई हैं कि यदि बच्चे को तनाव हो तो संपर्क करें। बच्चों के बचपन, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर एक बढ़िया नंबरों का सपना देश के ज्ञान-संसार पर भारी पड़ रहा है। विडंबना है कि डॉक्टर-इंजीनियर बनने जैसे सपने साकार करने के लिए लालायित कक्षा दस के बच्चे दस साल से स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई उनको असफलता का सामना करने का साहस नहीं सिखा पाती। बच्चे में अपने परिवार, शिक्षक के प्रति भरोसा नहीं पैदा हो पाता कि महज एक इम्तिहान के नतीजे के अच्छे नहीं होने से वे उसे ढांढ़स बंधाएंगे व आगे की तैयारी के लिए साथ देंगे। परीक्षा देने जा रहे बच्चे खुद के याद करने से ज्यादा इस बात से ज्यादा चिंतित दिखते हैं कि उनसे बेहतर करने की संभावना वाले बच्चों ने ऐसा क्या रट लिया है जो उसे नहीं आता। असल में प्रतिस्पर्धा के असली मायने सिखाने में पूरी शिक्षा प्रणाली असफल ही रही है। अपनी क्षमता के अनुरूप सबसे बेहतर करूं यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, लेकिन आज की प्रणाली दूसरों से तुलना में अपनी क्षमता आंकने का पाठ पढ़ाती है।
शिक्षा की प्रासंगिकता का सवाल
नई शिक्षा नीति को आये तीन साल हो गए लेकिन अभी तक जमीन पर बच्चे न तो कुछ नया सीख रहे हैं और न ही जो पढ़ रहे हैं उसका आनंद ले पा रहे हैं- बस एक दबाव है कि परीक्षा में जैसे-तैसे अव्वल या बढ़िया नंबर आ जाएं। कई बच्चों का खाना-पीना छूट गया है। कक्षा 10वीं के बच्चों को अंक नहीं, ग्रेड देने का काम कई साल से चल रहा है लेकिन बच्चों पर दबाव में कोई कमी नहीं। जो शिक्षा बारह साल में बच्चों को विषम परिस्थिति में अपना संतुलन बनाना न सिखा सके, वह कितनी प्रासंगिक व व्यावहारिक है?
 केवल नंबरों की दौड़
केवल नंबरों की दौड़
बारहवीं बोर्ड के परीक्षार्थी बेहतर स्थानों पर प्रवेश के लिए चिंतित हैं तो दसवीं के बच्चे अपने पसंदीदा विषय पाने के दबाव में। दूसरी ओर हैं मां-बाप के सपने। बचपन, शिक्षा, सीखना सब कुछ इम्तिहान के सामने गौण है। नंबरों की दौड़ में सब कुछ दांव पर लग गया है। क्या किसी बच्चे की योग्यता का पैमाना महज अंकों का प्रतिशत है? वह भी उस परीक्षा प्रणाली में, जिसकी मूल्यांकन प्रणाली संदेहों से घिरी है। मूल्यांकन का आधार बच्चों की योग्यता न हो कर उसकी कमजोरी है।
छोटी कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया के लगातार नीरस होते जाने व बच्चों पर पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के इरादे से मार्च 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के शिक्षाविदों की एक समिति बनाई थी, जिसने रिपोर्ट जुलाई 1993 में सरकार को सौंप दी कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से अधिक बुरा है न समझ पाने का बोझ। सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया लेकिन फिर उसकी सुध किसी ने नहीं ली। परीक्षा का वर्तमान तंत्र आनंददायक शिक्षा के रास्ते में रोड़ा है। इसके स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अव्वल आने की गला काट में न जाने कितने बच्चे कुंठा का शिकार होकर अतिवादी कदम उठा चुके हैं।
नैसर्गिक विकास में बाधा
परीक्षा व उसके परिणामों ने एक भयावह सपने, अनिश्चितता की जननी व बच्चों के नैसर्गिक विकास में बाधा का रूप ले लिया है। कहने को तो अंक सूची पर प्रथम श्रेणी दर्ज है, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों ने भी दरवाजों पर शर्तों की बाधाएं खड़ी कर दी हैं। सवाल है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है- परीक्षा में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना, विषयों की व्यावहारिक जानकारी देना या फिर नौकरी पाने की कवायद? निचली कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार हर साल अपनी रिपोर्ट में ड्रॉप आउट की बढ़ती संख्या पर चिंता जताती है। लेकिन कभी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अपने पसंद के विषय या संस्थान में प्रवेश न मिलने से कितनी प्रतिभाएं कुचल दी गई हैं। डिग्री पाने वालों में कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी पसंद के विषय पढ़े हैं?
दरअसल, आजादी के बाद शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य और पाठ्यक्रम के लक्ष्य एक-दूसरे में उलझ गए। बच्चों की बौद्धिक समृद्धि व जीवन की चुनौतियों से निबटने की क्षमता के विकास के लिए नंबरों की अंधी दौड़ पर विराम लगाने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है।