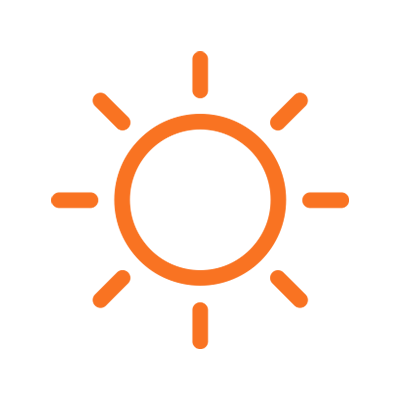कृष्ण प्रताप सिंह
हिन्दी भाषा, खासतौर पर उसके शब्दों व सामाजिक-साहित्यिक पत्रकारिता का अब तक जो भी संस्कार या मानकीकरण संभव हो पाया है, उसके पीछे उसके उन्नयन हेतु अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले स्वाभिमानी सम्पादकों की समूची पीढ़ी की अहर्निश सेवाओं की बड़ी भूमिका रही है। यह बड़ी भूमिका हिन्दी पत्रकारिता के ‘शिल्पकार’ और ‘भीष्म पितामह’ कहलाने वाले मराठी भाषी बाबूराव विष्णु पराड़कर (16 नवंबर, 1883-12 जनवरी, 1955) से बहुत पहले से दिखाई देने लगती है। दरअसल, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिन्दी पत्रकारिता को जनजागरण का अस्त्र बनाकर विदेशी सत्ताधीशों की नाक में दम करने और स्वतंत्रता के बाद नये भारत के निर्माण के लिए उन्होंने खुद को क्रांतिकारी शब्दशिल्पी बनाया।
यदि नहीं बनाया होता तो उनके वक्त स्थिरीकरण व मानकीकरण के दौर से गुजर रही हिन्दी भाषा और पत्रकारिता अनेक ऐसे शब्दों व सम्पादकों से वंचित रह जाती, जिनके बगैर आज वह काम नहीं चला पाती। श्री, सर्वश्री, राष्ट्रपति और मुद्रास्फीति जैसे अनेक शब्द, जिनका आज हिन्दी पत्रकारिता में धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है, उन्होंने ही हिन्दी को दिये।
उनका सबसे बड़ा पत्रकारीय योगदान यह है कि वे सम्पादक नामक संस्था की सर्वोच्चता के लिए जिद की हद तक सतर्क रहे। एक समय जब पराडकर जी उन दिनों के प्रतिष्ठित दैनिक ‘आज’ के सम्पादक थे, उसके संस्थापक और मालिक शिवप्रसाद गुप्त से मतभेद होने पर भी उन्होंने सम्पादकीय सर्वोच्चता से समझौता करना गवारा नहीं किया। उलटे उसे छोड़कर चले गये और बाद में शिवप्रसाद गुप्त के बहुत मनाने पर इस शर्त पर लौटे कि पत्र की सामग्री के चयन में उनका फैसला ही अंतिम हुआ करेगा।
साहित्यिक पत्रकारिता की बात करें तो अपने वक्त की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका ‘सरस्वती’ के सम्पादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी (9 मई, 1864-21 दिसम्बर, 1938) की उसे उत्कृष्ट बनाये रखने की जिद हमेशा बनी रही। कहते हैं, एक सज्जन ने उन्हें अपनी कविताएं भेजीं और अरसे तक उनके न छपने पर याद दिलाया कि ‘मैं वही हूं, जिसने एक बार आपको गंगा में डूबने से बचाया था’, तो अाचार्य द्विवेदी का जवाब था : आप चाहें तो मुझे ले चलिये, मुझे गंगा में वहीं फिर से डुबो दीजिए, जहां आपने डूबने से बचाया था, लेकिन मैं ये कविताएं सरस्वती में नहीं छाप सकता।’
इतना ही नहीं, जो मैथिलीशरण गुप्त अब राष्ट्रकवि कहलाते हैं, एक समय उनकी कविताएं उन्होंने यह कहकर छापने से मना कर दी थीं कि ‘सरस्वती’ खड़ी बोली की पत्रिका है और वे ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं। इसके बाद गुप्त ने उन्हें खड़ी बोली की कविताएं भेजीं, लेकिन अपना ब्रजभाषा वाला रसिकेन्द्र नाम ही लिखा, तो भी उन्हें फटकार ही मिली : ‘रसिकेन्द्र का जमाना चला गया’। फिर आचार्य ने उन्हें पत्र लिखा- आप ‘सरस्वती’ में लिखना चाहें तो इधर-उधर अपनी रचनाएं छपाने का विचार छोड़ दीजिए। जिस कविता को हम चाहें, उसे छापेंगे। लेकिन जिसे न चाहें, उसे भी न कहीं दूसरी जगह छपाइये, न किसी को दिखाइये, ताले में बन्द करके रखिये। अपना लिखा सभी को अच्छा लगता है परंतु उसके अच्छे-बुरे का विचार दूसरे लोग ही कर सकते हैं।’ उनकी यह जिद ‘रसिकेन्द्र’ को मैथिलीशरण गुप्त बनाकर ही तुष्ट हुई।
अलबत्ता, ‘अस्थिरता’ के बदले ‘अनस्थिरता’ शब्द के पक्ष में बालमुकुन्द गुप्त से हुए लम्बे विवाद में पूरी शक्ति लगाकर भी आचार्य न उसका औचित्य सिद्ध कर पाये, न ही उसे प्रचलन में ला पाये। लेकिन ‘सरस्वती’ ‘भारतमित्र’ और ‘हिन्दी बंगवासी’ आदि पत्रिकाओं में उसको लेकर चले लम्बे विवाद से इतना तो हुआ ही कि लेखक और सम्पादक भाषा और वर्तनी की एकरूपता व व्याकरण सम्मतता के प्रति पहले से ज्यादा सचेत रहने लगे। उन्हीं की ‘सरस्वती’ से निकले गणेश शंकर विद्यार्थी (26 अक्तूबर, 1890-25 मार्च, 1931) अपने द्वारा सम्पादित ‘प्रताप’ के मुखपृष्ठ पर उसके मास्टहेड के ठीक नीचे उनका रचा यह दोहा छापते थे : ‘जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है।’ विद्यार्थी का जज्बा ऐसा था कि उन्होंने ‘प्रताप’ के प्रवेशांक में घोषणा की थी : ‘समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परमोद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी साधन हम भारतवर्ष की उन्नति को समझते हैं।’
यह जज्बा इस सम्पादकीय नैतिकता तक जाता था कि उन्होंने 1930 में गोरखपुर में हुए हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो ‘प्रताप’ में उसकी रपट के साथ उसका चित्र छापने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसमें वे भी शामिल थे और प्रताप में उसके सम्पादक का चित्र छापने या उसका महिमामंडन करने की सर्वथा मनाही थी। वे ‘प्रताप’ में छपने वाले एक-एक अक्षर की नैतिक व वैधानिक जिम्मेदारी खुद स्वीकार करते थे और जेल जाने की कीमत पर भी उसके लेखक या संवाददाता का नाम कतई नहीं बताते थे। मिथ्याभिमान से भी उन्हें सख्त एलर्जी थी। ‘विशाल भारत’ के बहुचर्चित सम्पादक बनारसीदास चतुर्वेदी (24 दिसम्बर, 1892-02 मई, 1985) की वृत्ति और भी स्वतंत्र व विशिष्ट थी। उनके प्रायः सारे सम्पादकीय फैसलों की एक ही कसौटी थी : क्या उससे देश, समाज उसकी भाषाओं और साहित्यों, खासकर हिन्दी का कुछ भला होगा या मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्चतर मूल्यों की प्रतिष्ठा होगी अथवा नहीं।