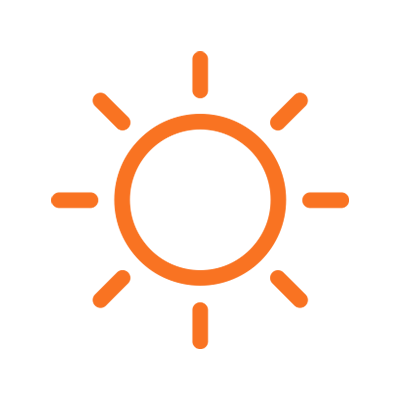आश्वासन और गारंटी में क्या अंतर होता है? भारतीय राजनीति के संदर्भ में इस प्रश्न का एक ही उत्तर है–जब कोई राजनेता कुछ करने का आश्वासन दे अथवा किसी काम की गारंटी दे तो इसका अर्थ है कि या तो वह आपको मूर्ख समझता है या मूर्ख बना रहा है। जनता को भरमाने के लिए आश्वासनों के ढेर तो अक्सर लगाए जाते रहे हैं और अक्सर देश की जनता ने इन आश्वासनों को ‘चुनावी जुमला’ मात्र पाया है, पर अब हमारे चतुर राजनेताओं ने एक नया शब्द काम में लेना शुरू किया है –गारंटी। अब नेता ‘गारंटी’ दे रहे हैं कि जनता यदि उन्हें सत्ता सौंपती है तो वे उसके जीवन में फलां-फलां बदलाव ला देंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो इस गारंटी के पूरा होने की गारंटी भी देते हैं।
कानून की भाषा में गारंटी का सामान्य अर्थ तो यही है कि यदि गारंटी पूरी न हुई तो गारंटी देने वाला कुछ हर्जाना भरेगा। लेकिन आज तक किसी नेता को ऐसा कोई हर्जाना भरते हुए देखा तो नहीं गया, हां, ऐसे आश्वासनों और गारंटियों से मतदाता छला अवश्य जाता रहा है। सच बात तो यह है कि नेता भी जानते हैं कि वह जनता को झांसा दे रहे हैं और जनता भी समझती है कि उसे भरमाने की कोशिश हो रही है। रूसी नेता निकिता ख्ाुश्चेव ने एक बार कहा था, ‘सब राजनेता एक से होते हैं, वे वहां भी पुल बनाने का आश्वासन दे सकते हैं जहां नदी ही न हो!’ रूसी नेता ने शायद यह बात अपने देश के संदर्भ में कही हो, पर यह बात हमारे देश पर भी लागू होती है। आश्वासन दावे, वादे, गारंटियां आज हमारी राजनीति का एक अविभाज्य हिस्सा बन गये हैं… और चुनावी मौसम में तो इन सब की भरमार हो जाती है। न कोई नेता यह बताता है कि उसके पिछले वादों का क्या हुआ और न मतदाता यह पूछने की ज़रूरत समझता है कि पिछले वादे पूरे क्यों नहीं हुए और उनके वादों-आश्वासनों पर क्यों विश्वास किया जाये। पर शायद भीतर ही भीतर राजनेता यह समझने लगे हैं कि मतदाता में उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब हमारे नेता आश्वासन नहीं देते, गारंटी देते हैं। हज़ारों-लाखों की उपस्थिति वाली सभाओं में छाती ठोक कर हमारे नेता गारंटियों की बौछार कर रहे हैं। वे यह भी मान रहे हैं कि वह जितना जोर से बोलेंगे जनता उनकी बात पर उतना ही ज़्यादा विश्वास करेगी!
ज़ोर से बोलने की इस प्रतिस्पर्धा में कोई नेता पीछे नहीं रहना चाहता। वह यह भी मानकर चल रहा है कि जैसे पिछले आश्वासनों को आम जनता भूलती रही है, वैसे ही गारंटियों को भी भूल जायेगी। पर सवाल आश्वासनों और गारंटियों को याद रखने और भूलने का नहीं है, सवाल हमारी समूची राजनीति पर लगातार लग रहे सवालिया निशानों का है। हमारी समूची राजनीति आज कठघरे में है, हमसे जवाब मांग रही है कि हमने उसे यानी राजनीति को नेताओं के भरोसे ही क्यों छोड़ दिया है? क्यों हम ऐसे नेताओं की बात पर विश्वास कर लेते हैं जो या तो जनता को मूर्ख समझते हैं, या मूर्ख बनाते हैं? हर पार्टी का हर नेता सिद्धांतों और मूल्यों की दुहाई देता है, अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से उजली बताने के दावे करता है। हकीकत यह है कि हमारी आज की राजनीति का सिद्धांतों-मूल्यों से कोई रिश्ता नहीं रह गया, और हकीकत यह भी है कि सारी कमीजें मैली हैं। हमारी राजनीति का यह हाल इसलिए हो गया है कि हमने इसे राजनेताओं के भरोसे छोड़ दिया––उन राजनेताओं के जिन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि कल उन्होंने क्या बोला था, और आज क्या कह रहे हैं! कल जिस बात को ग़लत ठहरा रहे थे, आज वही बात उन्हें सही लगने लगती है। सच तो यह है कि राजनीतिक नफे-नुकसान के इस घटिया खेल में हमारे राजनेताओं ने जनता को अपनी चाल का मोहरा मात्र समझ लिया है। यह सही है कि कभी-कभी ‘यह जनता है, सब जानती है’ का स्वर भी सुनाई पड़ जाता है, पर कुल मिलाकर स्थिति यही बनी हुई है कि राजनेता जनता को अपने खेल का खिलौना समझते हैं। अब समय आ गया है कि जनता राजनेताओं के हाथों का खिलौना बने रहने से इंकार करे।
देश के मतदाता को इस बात को समझना ही होगा कि जनतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति बहुत गंभीर मसला है, इसे नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जनता को समझना यह भी है कि उसे नेताओं की कथित गारंटियों के भरोसे नहीं, अपनी समझ के भरोसे अपने वोट का इस्तेमाल करना है। उसे देश के नेताओं से पूछना ही पड़ेगा कि उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है, और क्यों वह यह मानकर चल रहे हैं कि जनता को हमेशा मूर्ख बनाया जा सकता है। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सब पार्टियों का है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि पिछले 75 सालों में हमारी राजनीति का मूल्यों-आदर्शों से रिश्ता लगातार कमजोर हुआ है। सिद्धांतों की राजनीति अब एक जुमला मात्र बनकर रह गयी है! अवसरवाद हमारी राजनीति का मूल मंत्र बन चुका है। राजनीति अब सत्ता हथियाने का खेल बनकर रह गयी है। सत्ता के लिए राजनीति का यह घिनौना खेल जनतांत्रिक मूल्यों को नकारने वाला है।
जनतंत्र का मतलब पांच साल में एक बार वोट मांगना या वोट देना ही नहीं होता। जनतंत्र एक जीवन-प्रणाली है। राजनीतिक ईमानदारी इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। यह ईमानदारी कहीं खो गयी है। नहीं, खोई नहीं है, हम जान-बूझकर इस चाबी को कहीं रख कर भूल गये हैं। जनता को यह चाबी अपने हाथ में लेनी ही होगी। हमें अपने नेताओं से पूछना ही होगा कि उनकी कार्य-प्रणाली में ईमानदारी के लिए कोई जगह क्यों नहीं है? सिद्धांतों, मूल्यों और नीतियों के आधार पर राजनीतिक दल क्यों नहीं बनाये और चलाये जा सकते? बेईमान और भ्रष्ट राजनेताओं की राजनीतिक नफे-नुकसान के लिए दलों में आवा-जाही को क्यों स्वीकारा जाये? क्यों ऐसे राजनेताओं को अपना बना लिया जाता है जिन्हें कल तक भ्रष्टाचारी और बेईमान घोषित किया जाता रहा था? ऐसे में उन गारंटियों पर विश्वास क्यों किया जाये जो हमारे राजनेता खुले-हाथ लुटा रहे हैं?
जब बोलना ज़रूरी हो तो चुप रहने का कोई अर्थ नहीं होता, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। अब सच्चाई और ईमानदारी के पक्ष में बोलने की ज़रूरत है। यह आवाज़ उठानी ही चाहिए कि झूठे दावों-वादों वाली राजनीति अब स्वीकार नहीं होगी। उस बैंक के नाम की गारंटी का कोई मूल्य नहीं होता जिसकी साख जर्जर होती जा रही है–हमारी राजनीति ऐसा ही बैंक न बन जाये, यह गारंटी हमें, हर जागरूक नागरिक को, स्वयं को देनी ही होगी।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।